जलता चूल्हा
किस चूल्हे पर दिन रखूं..
किस राख में रात दबाऊं..
जिंदगी तो धूप में सिक गई..
अब तो बस खुरचन बची है..
तमाम दिन और रात की..।
खुरचन भी जली हुई है चूल्हे पर..
अब ये किसी का निवाला नहीं..
न किसी की तृप्ति..
बस अतीत में खोई..
खुद को ढूंढ रही है..
भरी परात में झांक..।
ज़ख्म ये बहुत पुराना है..
जिंदगी की भट्टी में जल..
काला हुआ है..।
एहसास बोझिल..
आवाज धीमी..
मन भारी हुआ है..।
तमाम दिन, तमाम राते..
अब खुद का हिसाब लगा रही है..
सलवटों में खुद को तलाश रही है..।
कांच के फ्रेम पर उंगलियां फिरा
अतीत में झांक रही है।
दिन चूल्हे में, रात राख में..
जिस्म मर्तबान में बंद हो तड़प गया..।
परम्पराओं को ढोती..
उजली स्त्री...काली हो..
वक्त की शूली पर..
बेवक़्त काल का ग्रास हो..
राख हुई..!!
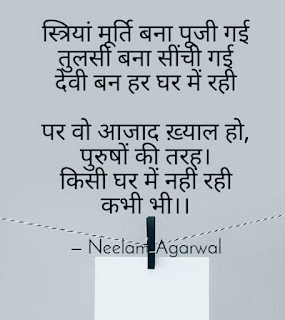


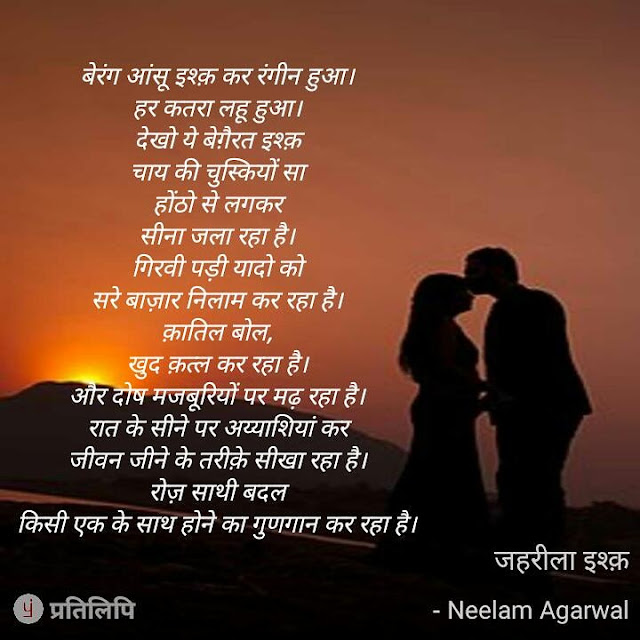
टिप्पणियाँ
एक टिप्पणी भेजें